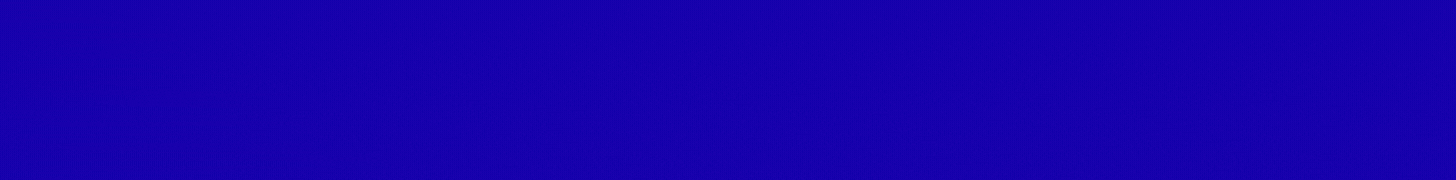पत्रकारिता एक शब्द, जो नि:शब्द है। खामोश है। चुप है। वह खुद की शर्मिंदगी में जकड़ा है। उसकी जर्जरता, बाहर निकलने की टीस में जिंदा है। उस तेज धूप की तलाश में है, जिसकी पहली सुबह से पत्रकार जागेंगे…रात जाएगी और नव विहान होगा। किरणों की आहट से आज के नौजवान पत्रकारों की आंखें खुलेंगी…नई हवा से ताकत मिलेंगी। खुद को सही मायने में पत्रकार कहने, कहलाने का भरोसा जगेगा और वह इसकी मौजूदगी को, खुद को परिभाषित कर सकेंगे…करेंगे।
खुद शर्म में डूबा यह पत्रकारिता किसकी भला कर पाएगा भला? नुकसान किसका? खुद पत्रकारिता का? जो पहले से कटघरे में है। जंजीरों से बंधा है? उसकी जुबां बंद है? चेहरे पर पट्टी लगी है? जीभ को बाहर निकालने की आजादी नहीं है? उसकी निर्विकार सोच में खलल डालने की साजिशन फरोसी हो रही? उसे सच बोलने, सच लिखने की छूट नहीं है? वह बंद मुट्ठी में है, जिसकी खोल में उसके नफस तिलमिला रहे हैं। जिसकी आग की झुरझुरी की चुभती-फड़फड़ाती सांसों को मरोड़, पत्रकारिता के जिस्म को काट दिए गए हैं। चुभती नस्तरों से इतने वार हुए हैं, गोया…पहले दर्द कम न थे जिस्म ये दामन में, कुछ और मुनाफा कर गए जो हमदर्द थे।
ऐसे में, कोशिश और मंशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। पत्रकारिता मरे, उसका कत्ल हो और उसका जश्न मनें। एक उत्साह हो। मगर शर्त्त यही, पहले से गर्म और लहू के कतरों को समेटे लहूलुहान, मरणासन्न, जीर्ण-शीर्ण, खोखली हो चुकी पत्रकारिता और उसके तथाकथित रखवालों की अर्थी भी ना निकले। बस श्राद्ध-कर्म हो जाए। ब्राह्णाणों का भोज हो। कर्मकांडी कंटाह के सामने पत्तल बिछ जाए। और, उसके बाद कौवे और चील उसे नोंचे, खसोटे…शेष बची हड्डियों का अवशेष भी तनिक ना छोड़े, बचे, दिखे। सब मिट्टी में स्वाह हो जाए।
वो पत्रकारिता, जो कभी स्वस्थ, निर्भीक, अनुशासित, ईमानदारिता की रोशनाई में कलम घसीटने वालों ने किया भी…या करने की कोशिश रत्ती भर की, वह पत्रकार कौन हैं? कहां हैं? किस अवस्था में हैं? किसे पत्रकार होना चाहिए? कौन कहलाने की आच्छादित दृष्टिकोण रखता है? कहां से आया है? किस परिधि को पार करने की पात्रता रखता है? इसे समझने की जरूरत आज किसी को नहीं है? ना वह समझने की स्थिति में हैं, न उसकी स्पष्टता उसकी जरूरत को ही समझाने को ही कोई तैयार? यही वजह है, यहां भला कौन अपनी मर्ज़ी से जी रहा है, सभी इशारे तिरी नज़र से बंधे हुए हैं….तू आंका है, हमें पता है…मगर मैं तेरी गुलामी करूं या ना करूं यह मेरी मर्जी है…इसे समझने को यहां कोई तैयार कहां….!
समुद्र सी विशालकाय क्षेत्रफल में फैले पत्रकारिता का लोगो किसके पास है? कौन बक रहा? कौन लिख रहा? किसे लिखना चाहिए? कौन लिखने की योग्यता रखता है?
मानो, वह देवघर का एक जनप्रतिनिधि, केनमनकाठी पंचायत के पूर्व मुखिया अमरनाथ दास सरीखे हो जो मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ अभद्रता करता, मां सरस्वती की मूर्ति से ही सेक्स करता दिखे। ऐसी प्रवृत्ति रखने वालों से परहेज कौन करेगा? उसे सूली पर चढ़ाने की कोशिश भी कौन करेगा? मुर्दे पैग़ंबर की मौत पर सभाएं बुलाएगा कौन? ‘दिवस’ मनाता हुआ, सार्वजनिक आंसू बहाता हुआ…दिखेगा कौन?, नींद को जगाता हुआ, अर्द्ध-सत्य थामे चिल्लाएगा कौन?
पत्रकार बनने की प्रवृत्ति ने उस पत्रकारिता को नष्ट करने पर आतुरता के साथ खड़ा है, जहां जिज्ञासा नहीं है? सिर्फ कुछ पाने की चाह है? उस सिस्टम के आगे झुकने की प्रवृत्ति है, जहां से पत्रकार कहलाने भर से भीख की गुंजाइश बढ़ती जा रही। भष्मासुर बने पत्रकार अपनी ही कोख को राख में समेटने पर आतुर हैं।
इसका फलसफा आए दिन दरभंगा की पत्रकारिता में मिलता-दिख रहा। जहां, गोबरचपोत होती पत्रकारिता का जिम्मेदार कौन है! कोई कह नहीं सकता…जिम्मेदारी लेने को कतई तैयार नहीं…मगर, हम हर दिन अविश्वास-सी प्रखर की जद में हैं, यह सोच लो। किसकी तलाश करूं किसे बंद रखूं।
वर्तमान की पत्रकारिता को केंद्र में रखूं। भविष्य की स्पष्ट और सुनिश्चित पत्रकारिता की कद्र करूं। उसकी दीर्याघु जीवन की कामना करना सीखूं या फिर उसे मारने पर उतारू हों जाऊं। मगर, पहले खुद कैसे जिंदा रहोगे…सोच लो।
कारण, सीधी रोशनी पड़ती दिखती नहीं कही। क्षत-विक्षत लाशों के पास, आखिर बैठे रहेंगे कबतलक असंख्य मुर्दे उदास देख लो। गोलियों की ज़ख्म देह पर नहीं पड़ती, रक्तस्राव अस्थिमज्जा से नहीं हो रहे, सिर्फ एक काग़ज़ का नक्शा है-ख़ून छोड़ता हुआ और तुम वहीं पत्रकारिता करोगे…उसी खून से…आखिर कब तलक? सोच लो।
पत्रकारिता को शब्द दो। उसे नि: शब्द मत करो। खामोशी को स्वर दो। गला मत टटोलो। खुद की शर्मिंदगी में जो पत्रकारिता पहले से दल-दल में है, उसे उबारो, बाहर निकालो, उसे और दफन मत करो। कफन की गुंजाइश मत तलाशो। मैंने चाहा था कि चुप रहूं, देखता जाऊं…सबकुछ निर्विकार, बिना चीखे…मगर…इस भीड़ में अकेले कब तलक परचम उठाओगे सोच लो।
दरभंगा में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ। पूरी दुनिया ने देखा। उसे छुपाकर, आवरण में कैद करने की नीयत रखने वालों से अनुरोध, ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसे कर्मियों को प्रशिक्षित करो, कम से कम उस तिरंगे की स्वाभिमान से आगे ना खेल सकें, इसकी पुख्ता व्यवस्था करो। खानापूरी करना मत सीखो। गलती को ढ़कना मत सीखो। उसे स्वीकारो और आगे गलती ना हो इसकी ताकीद करो। इससे बाहर निकलकर एक स्वस्थ और सभ्य कार्यसंस्कृति का विन्यास करो, जहां ऐसी हिमाकत की कोई गुंजाइश ही शेष ना रहे।
कितनी जगह से गलती को काटने की प्रवृत्ति करोगे। उससे गलती मिटाने की जिद करोगे। गलती मानवीय भूल है। गलती हर किसी से होती है। उसे स्वीकार करो। पत्रकारिता में भी गलतियां होती हैं। तत्काल पूरी दुनिया को पता चल जाता है, गलती हुई है। भूल सुधार छपा है।
मगर, ओहदेदार गलती कब स्वीकारेंगे? चंद पत्रकारिता की जमात से दुनिया को समेटने और चांद को रोटी समझने की भूल करने वाले हमेशा गरीबी की पृष्ठभूमि में ही जिंदा रहते हैं। स्वस्थ नहीं हो पाते।
स्वस्थ बनो। स्वस्थ रहो और स्वस्थ समाज की विस्तारित सोच को आगे विस्तार दो। उसे ताबूत में बंद कर उसपर कफन फेंकने की जिद मत करो।
दरभंगा की पत्रकारिता मरणासन्न अव्यवस्था में है। उसे और क्यों मारना चाहते हो? क्यों कुचलना चाहते हो? क्यों उसपर बर्बर कुल्हाड़ चलाना चाहते हो?
मगर करेगा कौन? सत्ता-प्रशासन के लंबे नाखूनों ने जिसका जिस्म नोच लिया! घुटनों पर झुका जो पहले से दिख रहा, वैसे भक्तों की फेहरिस्त तैयार करो। पत्रकारों ने उस तिरंगे में भी स्कोप तलाशा। इस स्कोप से पत्रकारिता बचेगी नहीं, मरेगी। मारना चाहते हो, एक दिन सामूहिक हवन करो, तिलांजलि दे दो।
सच मानो तो मनोरंजन ठाकुर (To be honest with Manoranjan Thakur) के साथ