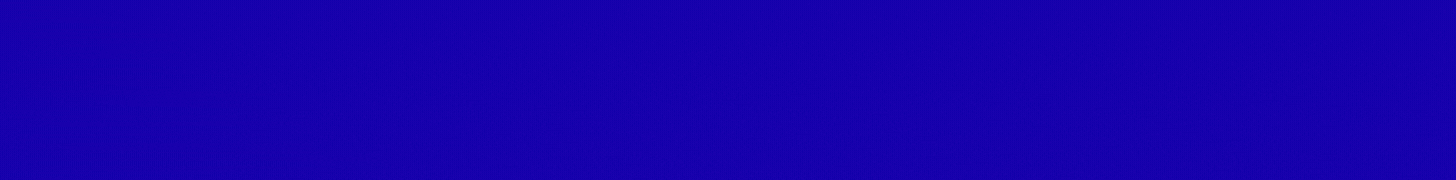UGC: सियासत की प्रयोगशाला में नीतियां कभी दम नहीं तोड़तीं, बस उनके नाम और कलेवर बदल दिए जाते हैं। आरक्षण का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, जिसे संविधान निर्माताओं ने समाज के उत्थान की एक अस्थायी सीढ़ी के तौर पर देखा था, लेकिन राजनीति ने इसे वोटबैंक का स्थायी राजमार्ग बना दिया है।
भारत में नीतियाँ कभी मरती नहीं—वे बस “अगले संशोधन” तक जीवित रहती हैं। आरक्षण भी ऐसा ही एक अध्याय है, जिसे संविधान निर्माताओं ने एक अस्थायी औषधि के रूप में लिखा था, पर राजनीति ने उसे स्थायी टॉनिक बना दिया। अनुच्छेद 334 के तहत राजनीतिक आरक्षण दस वर्षों के लिए था, पर हर दशक में उसकी “मियाद” बढ़ती रही। लगता है हमारी संसद में कैलेंडर बदलता है, पर संकल्प नहीं।
1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और देश में सामाजिक न्याय की राजनीति ने नई करवट ली। 27% OBC आरक्षण जुड़ा, पहले से मौजूद 22.5% SC/ST के साथ कुल 49.5% का गणित बना। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय कर संतुलन साधने की कोशिश की, मानो कह दिया हो—“न्याय हो, पर गणित भी बचा रहे।” बाद में EWS का 10% जुड़ गया और अब हालात यह हैं कि सामान्य वर्ग के हिस्से में बची सीटें ऐसी लगती हैं जैसे थाली में परोसी आख़िरी रोटी—जिस पर सबकी नज़र है।
राजनीति ने आरक्षण को सामाजिक उत्थान से ज़्यादा वोट-उत्पादन का औज़ार बना दिया है। हर चुनाव में “न्याय” का नया पैकेट आता है, और हर बार सामान्य वर्ग के युवाओं से कहा जाता है—“आप तो पहले से सक्षम हैं, थोड़ा और सह लीजिए।” पर सवाल है—कब तक? क्या मेरिट अब केवल भाषणों में ही सुरक्षित है?
13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम, 2026” जारी किए। उद्देश्य भेदभाव मिटाना बताया गया, पर मसौदा पढ़कर कई शिक्षकों और छात्रों को लगा कि यह समानता से ज़्यादा संदेह का दस्तावेज़ है। “इक्विटी कमेटियों” में कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य, पर सामान्य वर्ग का नाम गायब। “अप्रत्यक्ष भेदभाव” जैसी व्यापक परिभाषाएँ—जिनकी व्याख्या परिस्थिति से अधिक मनोदशा पर निर्भर हो सकती है। प्रारंभिक ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जो अंतिम संस्करण से रहस्यमय ढंग से ग़ायब हो गया।
29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए संकेत दिया कि अस्पष्ट प्रावधान समाज में विभाजन बढ़ा सकते हैं। यह टिप्पणी केवल विधिक नहीं, सामाजिक चेतावनी भी है।
व्यंग्य यह है कि समानता के नाम पर हम एक नया असमानता-सूत्र गढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं कि एक वर्ग को स्थायी सहारा और दूसरे को स्थायी संदेह दिया जाए। यदि नीति का लक्ष्य समरसता है, तो संवाद, पारदर्शिता और समयबद्ध समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।
सरकार को समझना होगा—न्याय की नाव वोटों की लहर पर चल सकती है, पर टिकती वही है जिसमें सबको संतुलन का भरोसा हो। अन्यथा, मेरिट की यह वनवास गाथा आने वाली पीढ़ियों के मन में एक स्थायी प्रश्नचिह्न छोड़ जाएगी।
आइए। रिपोर्ट को इस तरह भी जोड़ें।
UGC द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम, 2026” के मसौदे ने एक बार फिर इस बहस को सतह पर ला दिया है। इसका घोषित उद्देश्य तो भेदभाव मिटाना था, लेकिन इसके प्रावधानों ने योग्यता और समानता के बीच एक नई खाई खोदने का अंदेशा पैदा कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत राजनीतिक आरक्षण को केवल दस वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन हर दशक में यह “मियाद” किसी न किसी बहाने बढ़ती रही। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, जो पहले से मौजूद 22.5% एससी/एसटी कोटे के साथ मिलकर कुल 49.5% हो गया।
1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने 50% की सीमा तय करके एक संतुलन बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में EWS कोटे के 10% आरक्षण ने इस गणित को फिर से बदल दिया। अब हालात यह हैं कि सामान्य वर्ग की सीटें थाली की उस आखिरी रोटी जैसी हो गई हैं, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
UGC के ‘इक्विटी’ नियमों पर क्यों मचा है बवाल?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस नए मसौदे में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पर शिक्षाविदों और छात्रों ने गंभीर चिंता जताई है। ड्राफ्ट के अनुसार, संस्थानों में “इक्विटी कमेटियां” बनाई जाएंगी, जिनमें कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य होगा, पर सामान्य वर्ग का कोई जिक्र तक नहीं है। इसमें “अप्रत्यक्ष भेदभाव” जैसी अस्पष्ट परिभाषाएं शामिल की गई हैं, जिनकी व्याख्या तथ्यों से ज्यादा निजी धारणाओं के आधार पर हो सकती है। यह पूरी कवायद देश की मौजूदा आरक्षण नीति को एक नए और अधिक जटिल मोड़ पर ले जाती दिख रही है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ड्राफ्ट के शुरुआती संस्करण में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जिसे अंतिम मसौदे से हटा दिया गया।
इन्हीं चिंताओं को देखते हुए 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस तरह के अस्पष्ट प्रावधान समाज में सौहार्द बढ़ाने के बजाय विभाजन को और गहरा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चेतावनी है।
क्या सामाजिक न्याय के नाम पर योग्यता से समझौता?
यह एक कड़वा व्यंग्य है कि समानता स्थापित करने के नाम पर हम एक नई तरह की असमानता की नींव रख रहे हैं। सामाजिक न्याय का यह अर्थ कतई नहीं हो सकता कि एक वर्ग को स्थायी बैसाखी दी जाए और दूसरे वर्ग को स्थायी तौर पर संदेह की नजर से देखा जाए। यदि किसी भी नीति का अंतिम लक्ष्य एक समरस समाज का निर्माण करना है, तो उसमें सभी पक्षों के साथ संवाद, पारदर्शिता और एक निश्चित समय-सीमा के बाद उसकी समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। नीतियां ऐसी हों जो समाज को जोड़ें, तोड़ें नहीं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
सरकार को यह समझना होगा कि न्याय की नाव वोटों की लहरों पर कुछ दूर तो चल सकती है, पर टिकती वहीं है जिसमें सबको संतुलन का भरोसा हो। वरना, योग्यता की यह वनवास गाथा आने वाली पीढ़ियों के मन में व्यवस्था के प्रति एक स्थायी प्रश्नचिह्न बनकर रह जाएगी।